अंग्रेजों के दौर में काफल के फल का इस्तेमाल सिर्फ़ खाने के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी किया जाता था। सिर्फ़ कुमाऊँ से प्रत्येक वर्ष इस फल का लगभग पचास टन निर्यात किए जाता था। सारदा और जमुना नदी के बीच के भाग से लगभग 70 टन काफल के फल निर्यात होता थे। सिर्फ़ गढ़वाल से ही लगभग 1800 किलो निर्यात होता था। पहाड़ के इस फल के व्यापार और निर्यात पर ब्रिटिश सरकार को आठ आने (50 पैसा) प्रति मन (40 किलो) की दर से रॉयल्टी दी जाती थी जो कि बरसिंघे के खाल पर मिलने वाली रॉयल्टी के बराबर हुआ करती थी।
“काफल के निर्यात पर ब्रिटिश सरकार को आठ आने (50 पैसा) प्रति मन (40 किलो) की दर से कर वसूलती थी”
काफल के फल का निर्यात पहाड़ों से उत्तराखंड के लगभग सभी मैदानी क्षेत्रों में होता था जबकि इसके पेड़ के खाल का निर्यात ज़्यादातर हल्द्वानी, रामनगर, ब्रह्मदेव और कोटद्वार को किया जाता था। ये तीनो स्थान ही उस दौर का पारम्परिक औषधि केंद्र और व्यापार केंद्र भी हुआ करती थी।

आज का पहाड़ी समाज काफल फल के व्यापारिक-वाणिज्यक होने की कल्पना भी नहीं कर पता है। गाँव में रहने वाले लोग जंगल में पड़े इस फल को बिना किसी से पूछे तोड़कर खा सकते हैं। काफल उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई पर्वतीय राज्यों (हिमालय) समेत नेपाल, चीन, अफगनिस्तान, भूटान और सिंगापुर में भी मिलने वाला फल का पेड़ है जो जून-जुलाई के महीने में पकता है। काफल का जिक्र कई कुमाऊँनी और गढ़वाली लोककथाओं और लोकगीतों में मिलता है जिनमे “बेडु पाको बारमासा, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला” और “काफल पाक्यो, मील नी चाख्यो” प्रमुख है।
इसे भी पढ़े: “प्यारी पहाड़न” में कहां है पहाड़, पहाड़न या उसका रसोई?
काफल के फल को तो हम सब खाते हैं पर पुराने समय में जौनसार क्षेत्र में इसका शर्बत भी बनाया जाता था। इसके पेड़ के छाल को कृमिनाशक, उत्तेजक, त्वचा के लाली कम करने, ब्लड की गति बढ़ाने आदि में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल चमड़े की सफ़ाई में भी किया जाता था। स्थानीय लोग इसे मिर्गी की बीमारी में शरीर पर रगड़कर दवाई के रूप में इस्तेमाल करते थे।

गठिया बीमारी में इसके छाल का लेप भी लगाया जाता था। इसके अलावा काफल का इस्तेमाल कई औषधियों में मिश्रण के रूप में किया जाता था। 19वीं सदी में बोटनिकल सर्वे ओफ़ इंडिया के दावे के अनुसार जौनसार में इसका इस्तेमाल मछली को मारने के लिए ज़हर के रूप में भी किया जाता था हालाँकि आज स्थानीय लोग मछली मारने वाले दावे को भ्रामक मानते हैं।
इसे भी पढ़े: क्या है पहाड़ी कहावतों में छुपे मंडुवा (Finger Millets) से सम्बंधित इतिहास के राज?
स्त्रोत: 1) The Himalayan Gazetteer or The Himalayan District of North Western Province (in 3 volumes and 6 parts) by Edwin T Atkinson, 1882.
2) ‘Forest Flora of the School Circle’: An Analysis Compiled for the use of the Students of the Imperial Forest School, Dehradun, Published in 1901.
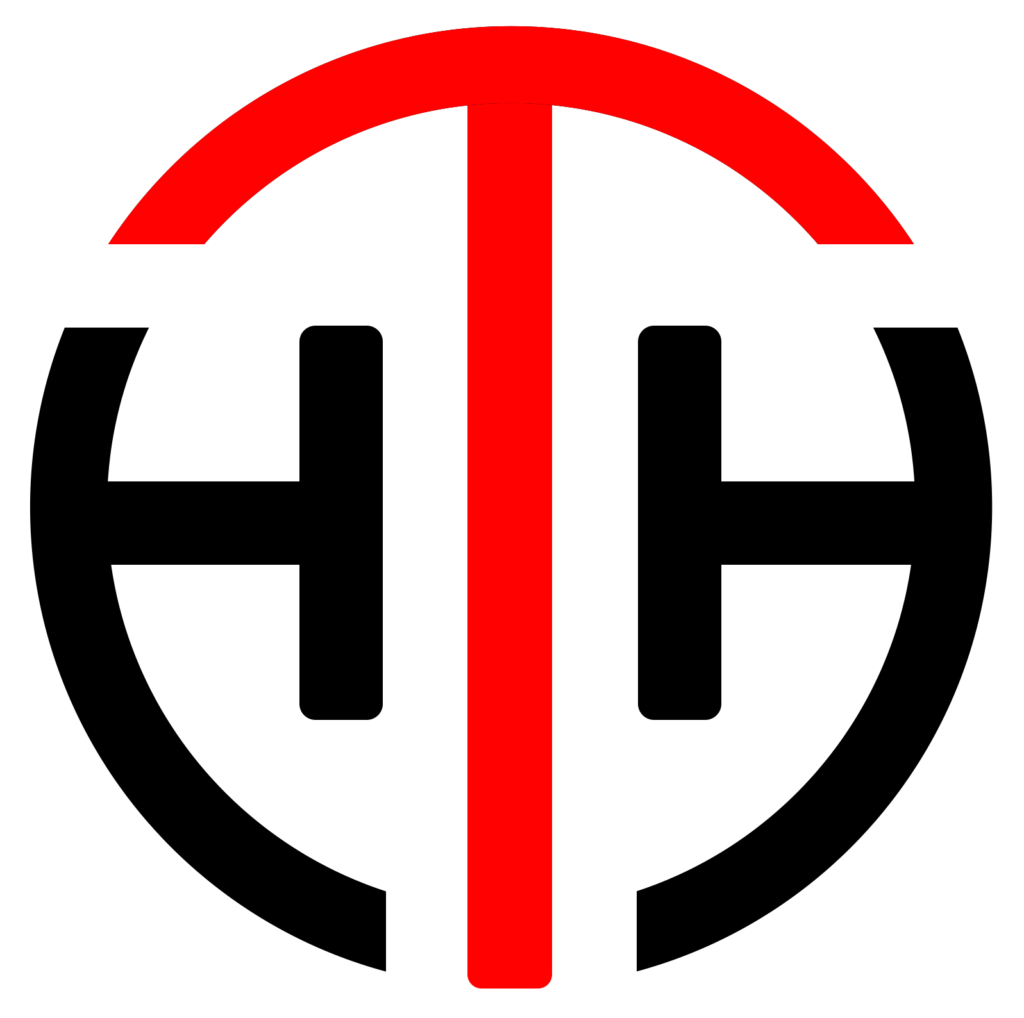
Hunt The Haunted के Facebook पेज से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें (लिंक)

